
आज के युग में मोबाइल लगभग सभी के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं. आज स्मार्ट फोन का जमाना है और हर किसी की इस तरफ तेजी से दिलचस्पी बढ़ती जा रही है. सभी उम्र के लोगों की उंगलियां स्मार्टफोन पर पूरे दिन थिरक रही हैं. स्मार्टफोन तो लोगों के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन की तरह काम कर रहे हैं. स्मार्टफोन के प्रभाव को कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि यह हमारे जीवन में आज चाबी और पर्स से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं.
बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 84 प्रतिशत स्मार्टफोन उपयोगकर्ता जागने के 15 मिनट के भीतर अपने फोन की जांच करते हैं. रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि जागने के समय का लगभग 31 प्रतिशत हिस्सा स्मार्टफोन पर व्यतीत होता है और लोग औसतन दिन में 80 बार अपने डिवाइस को चेक करते हैं. यह बहुत बड़ा और हैरान कर देने वाला आंकड़ा है. इस वजह से उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है जिस वजह से उन्हें जाने -अंजाने में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. हालांकि इसकी सुविधाएं कई मायनों में सहायक हैं परंतु इसका अत्यधिक उपयोग सृजनात्मकता और शैक्षिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है. शिक्षा के क्षेत्र में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने और मोबाइल पर निर्भरता को कम करने की दिशा में संतुलन स्थापित करना आज की महती आवश्यकता है.
कंटेंट मोनेटाइजेशन और मार्केटिंग टेक्नोलॉजी कंपनी इनमोबी ने साल 2024 की अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारतीय अपने स्मार्टफोन पर प्रतिदिन औसतन 4 घंटे से ज्यादा बिताते हैं. यानी कि पूरे साल में 1460 घंटे, साल के 12 महीने में 2 महीने सिर्फ स्माटफोन पर भारतीय औसतन खर्च कर रहे हैं. बीसीजी की एक अन्य स्टडी के मुताबिक, दो में से एक बार भारतीय लोग फोन का इस्तेमाल जरूरत के बजाय आदत के कारण करते हैं.
कई अध्ययन हुए जिनसे पता चला कि स्मार्टफोन के अत्यधिक सेवन से मानव शरीर में बहुत सारी बीमारियां जन्म ले रही हैं. स्मार्टफोन से निकलने वाले इलेक्ट्रोमेगनेटिक विकिरणों से डीएनए क्षतिग्रस्त हो सकता है. इसके अलावा मोबाइल का अधिक इस्तेमाल आपको मानसिक रोगी, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, डायबिटिज, ह्रदय रोग आदि कई बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से घेर सकता है. इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ 2022 के अनुसार, भारतीय छात्रों में 67% ने बताया कि स्मार्टफोन की वजह से उनका ध्यान भटकता है. रात में स्मार्टफोन उपयोग से नींद में कमी होती है ,जिससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है. स्मार्टफोन के अत्यधिक उपयोग से डिजिटल लत की समस्या हो सकती है. "स्मार्टफोन ओवरयूज एंड क्रिएटिविटी" शोध में पाया गया कि 73% छात्रों की कल्पनाशक्ति घटती है क्योंकि वे वास्तविक अनुभवों की जगह स्क्रीन पर निर्भर रहते हैं. NCERT की साल 2023 की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 14-18 आयु वर्ग के 33% छात्रों में "स्मार्टफोन एडिक्शन" की प्रवृत्ति देखी गई है. यह ऐसे आंकड़े हैं जो हमें रुकने और गौर करने पर मजबूर करते हैं. स्मार्टफोन हमारे और आपके सबसे कीमती समय को बेवजह खराब कर रहे हैं.
फ्रांसीसी दार्शनिक ब्लेज़ पास्कल ने साल 1654 में लिखा था कि "मानवता की सभी समस्याएं मनुष्य की अकेले एक कमरे में शांति से बैठने में असमर्थता से उत्पन्न होती हैं". उनके मुताबिक,हमें एक कमरे में अकेले चुपचाप बैठने की ज़रूरत है. व्यस्तता वास्तव में आध्यात्मिकता का दुश्मन है. हम सभी को अपने भीतर क्या हो रहा है. इस पर ध्यान देने के अनुशासन की जरूरत है अपनी आत्मा की जाँच करने के लिए कि हम वास्तव में कौन हैं. लेकिन स्मार्टफोन की दुनिया में यह समस्याएं और भी बदतर हैं. क्योंकि जब हम चुप रहना चाहते हैं तब भी व्हाट्सएप संदेशों, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया पर महिमामंडन की अप्रिय इच्छा से घिरे रहते हैं. वास्तव में हम जानते हैं कि हम वाकई में क्या अच्छा कर रहे हैं?
हमारे समय के अधिकांश महान आविष्कार, सिद्धांत, कलाकृतियाँ और अन्य सभी की कल्पना और परिकल्पना तब की गई थी जब उनके रचयिता शांत समय बिता रहे थे.ध्यान कर रहे थे. गहराई से चिंतन कर रहे थे. आइज़ैक न्यूटन और सेब एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं. आज हम शायद ही ऐसा करते हैं. क्या हमने इस बारे में कभी सोचा है? हमारे जीवन का बड़ा हिस्सा तकनीकी उपकरणों ने घेर रखा है जिससे हमारी रचनात्मकता और सृजनात्मकता पर गहरा प्रभाव पड़ा है.
आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है. संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 10 से 24 वर्ष के आयु वर्ग में लगभग 37 करोड़ युवा है. यह देश की कुल जनसंख्या का 26% हिस्सा हैं. इसके अतिरिक्त, 15 से 64 वर्ष के आयु वर्ग में लगभग 97 करोड़ लोग हैं जो कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं. वर्तमान समय में रोजमर्रा के कामकाज से लेकर जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में तकनीक बहुत अहम रोल निभा रही है लेकिन इसी तकनीक ने हमारे जीवन जीने के तरीके को आसान बनाया है तो कई तरह की परेशानियों को भी न्यौता दिया है.
लेकिन क्या आपने सोचा है तकनीक के प्रभाव के कारण आजकल बहुत से छात्र रचनात्मक होने से क्यों डरते हैं? प्रौद्योगिकी छात्रों के दिमाग पर हावी हो रही है जिससे वे रचनात्मक रूप से सोचने में असमर्थ हो रहे हैं. मुझे यह समझ नहीं आता कि छोटी-छोटी जीवन से जुड़ी सामान्य चुनौतियों का हल खोजने के लिए इंटरनेट का सहारा लेना कहां तक सही है? असाइनमेंट, टास्क, होम वर्क को पूरा करने के लिए छात्र पाठ्य-पुस्तकों की जगह गूगल पर निर्भर हो गए हैं. सरल शब्दों में कहें तो, प्रौद्योगिकी का अत्यधिक उपयोग अकेले ही छात्रों की रचनात्मक क्षमता को नष्ट कर रहा है. लेकिन थोड़ी सतर्कता और जागरुकता से छात्रों और युवा आबादी को इस भंवर से निकाला जा सकता है. शिक्षक रचनात्मकता को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण कड़ी हैं. उनके थोड़े से प्रयास विद्यार्थियों में रचनात्मकता और तार्किकता का समायोजन कर सकते हैं.
सृजनात्मकता का महत्व
सृजनात्मकता केवल नई चीजें बनाने तक सीमित नहीं है. यह समस्याओं को हल करने, नई सोच विकसित करने और आत्म-अभिव्यक्ति के माध्यम से व्यक्तिगत विकास का मार्ग प्रशस्त करती है.
शिक्षा में सृजनात्मकता का विकास निम्न चरणों के तहत प्राप्त किया जा सकता है.
• व्यावहारिक शिक्षा का प्रयोग: विद्यार्थियों को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित न रखते हुए उन्हें प्रयोगों, परियोजनाओं और गतिविधियों में शामिल करना चाहिए.
• कलात्मक गतिविधियां: संगीत, चित्रकला, लेखन और नाटक जैसी कलात्मक विधाओं को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहिए.
• खुली सोच को बढ़ावा: विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों पर अपनी राय व्यक्त करने और नवाचार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए.
• मोबाइल की निर्भरता पर प्रहार: मोबाइल फोन, यदि विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग न किया जाए, तो यह समय की बर्बादी और मानसिक थकान का कारण बन सकता है। विद्यार्थियों की पढ़ाई और सृजनात्मक विकास में इसका नकारात्मक प्रभाव स्पष्ट है.
मोबाइल पर निर्भरता को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं.
• शिक्षा में डिजिटल अनुशासन: मोबाइल का उपयोग केवल शैक्षिक उद्देश्यों तक सीमित रखा जाए.
• ऑफ़लाइन गतिविधियों को प्रोत्साहन: खेल, समूह चर्चा और सामूहिक कार्यों को बढ़ावा देना चाहिए.
• डिजिटल डिटॉक्स: विद्यार्थियों को समय-समय पर मोबाइल से दूर रखने के लिए जागरूक किया जाए.
• स्मार्ट ऐप्स का चयन: सृजनात्मकता बढ़ाने वाले शैक्षिक ऐप्स का उपयोग कर मोबाइल का सकारात्मक रूप से प्रयोग किया जा सकता है.
• सृजनात्मकता और तकनीक में संतुलन: तकनीक और सृजनात्मकता को साथ लाने के लिए शिक्षकों और अभिभावकों को सामूहिक प्रयास करना होगा. विद्यार्थियों के समय प्रबंधन और मोबाइल उपयोग की आदतों पर ध्यान देना आवश्यक है.
• सृजनात्मक शिक्षा मंच: ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों प्रकार के मंचों का निर्माण, जो छात्रों को नए कौशल सीखने और सृजनात्मकता बढ़ाने के अवसर प्रदान करें.
• पारंपरिक और तकनीकी शिक्षा का मेल: पारंपरिक पाठ्यक्रमों को तकनीकी नवाचारों से जोड़कर सृजनात्मकता का पोषण किया जा सकता है.
सृजनात्मकता के विकास और मोबाइल निर्भरता को कम करना एक संतुलित दृष्टिकोण की मांग करता है. शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि व्यक्तित्व का समग्र विकास करना है. यदि विद्यार्थी सृजनात्मकता को अपनाते हैं और मोबाइल का विवेकपूर्ण उपयोग करते हैं तो वे न केवल शैक्षिक बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी सफल हो सकते हैं. संतुलन ही कुंजी है और यह संतुलन सृजनात्मक शिक्षा और तकनीक के संयोजन से प्राप्त किया जा सकता है. रचनात्मकता हमेशा कल्पना से शुरू होती है और इतिहास बताता है कि हम जिन चीज़ों की कल्पना करते हैं उनमें से कई चीज़ें बाद में अस्तित्व में आती हैं. जीन रॉडेनबेरी ने 1966 में स्टार ट्रेक फ़्लिप कम्युनिकेटर की कल्पना की और मोटोरोला ने 1996 में उनका उत्पादन किया. 1800 के दशक के मध्य में ऑगस्टा एडा किंग ने कंप्यूटिंग मशीनों के लिए एक ऐसी भाषा की कल्पना की जो अस्तित्व में भी नहीं थी. आज उन्हें आधुनिक प्रोग्रामिंग भाषाओं के संस्थापक के रूप में जाना जाता है.


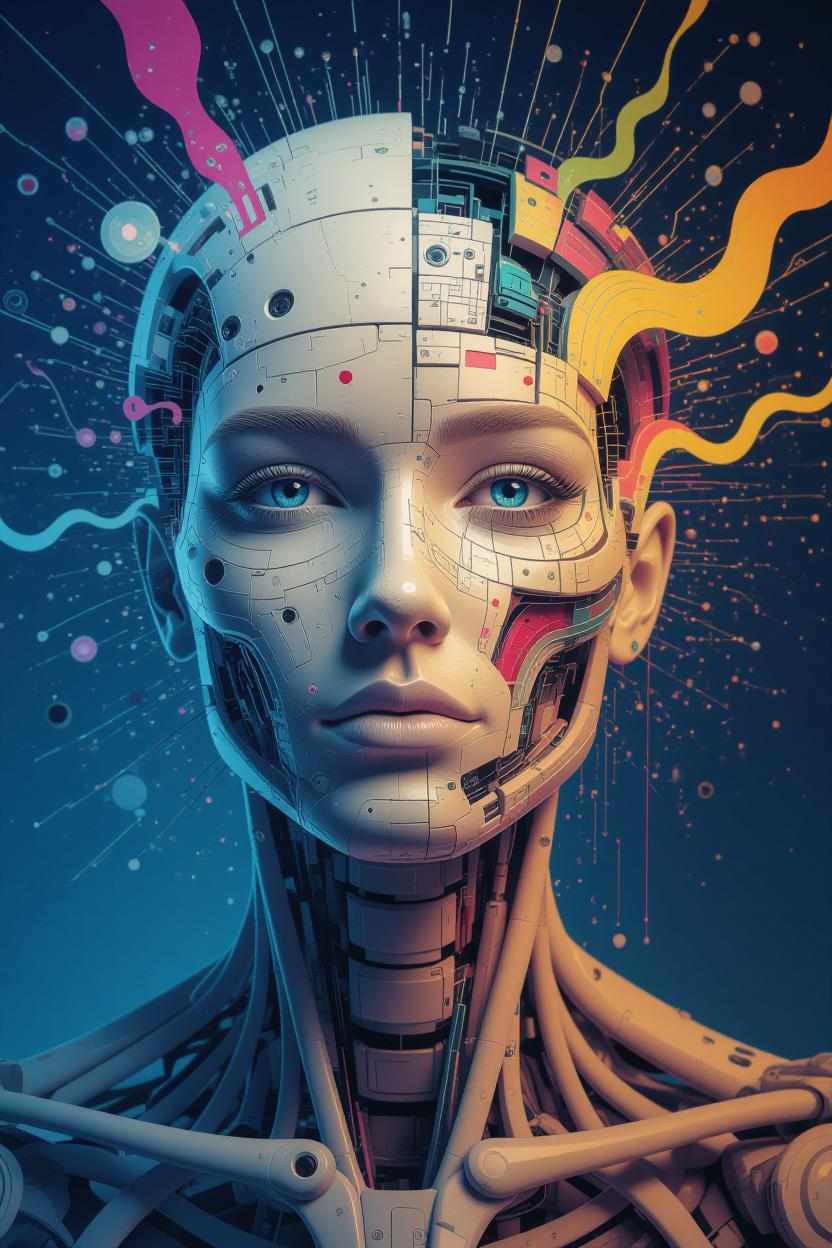












Write a comment ...